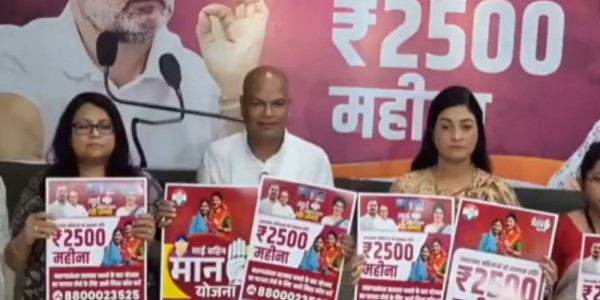रॉयटर्स ने देश-विदेश के कई बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से बात की, इनमे से 70 प्रतिशत से ज़्यादा ने कहा कि जून 2025 में सरकार ने जो बेरोज़गारी की दर 5.6% बताई वो हक़ीक़त से काफी दूर है।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के मुताबिक़, कुल बेरोज़गारों में से 82.90% नौजवान हैं। इससे बढ़कर पढ़े-लिखे नौजवानों की संख्या 65% है। ये बहुत पुराना तर्क है कि बेरोज़गारी और ग़रीबी की असली वजह है ज़्यादा आबादी। पूंजीपतियों के हित में बोलने वाले ‘बुद्धिजीवी’ इस भ्रम को बहुत ज़ोर-शोर से फैलाते हैं, और आम लोगों में भी इसे सच मानने का रुझान बन गया है। इस झूठी कहानी की नींव रखी थी थॉमस माल्थस ने एक अंग्रेज़ पूंजीवादी अर्थशास्त्री जिसने 1798 में ये थ्योरी पेश की।
PLFS रिपोर्ट: बेरोज़गारी का असली कारण ‘जनसंख्या’ नहीं
माल्थस ने कहा था कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है (1,2,4,8 के क्रम में जबकि खाने-पीने और ज़रूरतों के साधन धीरे-धीरे बढ़ते हैं 1,2,3,4 उसके मुताबिक, यही अंतर ग़रीबी और बेरोज़गारी की असली वजह है। यानी ग़रीब खुद ही अपनी हालत के ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और संसाधन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते। माल्थस ने ये तक कहा था कि बाढ़, अकाल और महामारी जैसी आपदाएँ दरअसल ‘फायदेमंद’ होती हैं क्योंकि ये ‘ग़रीब आबादी’ को कम कर देती हैं। ये सोच सिर्फ़ अमानवीय ही नहीं, बल्कि जानबूझकर ग़रीबों को दोषी ठहराने वाली साजिश थी। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब (Das Kapital) में इस पूरे ‘माल्थस सिद्धांत’ को वैज्ञानिक रूप से नकार दिया था।
मार्क्स ने समझाया कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का जमावड़ा कुछ गिने-चुने हाथों में होता है। और मुनाफ़े की होड़ में पूंजीपति मज़दूरों की मेहनत को लूटते हैं, फिर उसी से ज़्यादा मशीनें, नई तकनीकें और तेज़ उत्पादन शुरू करते हैं। इस दौड़ में, कुछ वक़्त के लिए रोज़गार तो बढ़ता है लेकिन धीरे-धीरे तकनीक के ज़रिए कम मज़दूरों से ज़्यादा काम निकाला जाता है। यानी कम तनख्वाह, ज़्यादा मेहनत और बची हुई आबादी बेकार बैठ जाती है। इसी प्रक्रिया में पैदा होती है ‘सापेक्ष अतिरिक्त आबादी’ (Relative Surplus Population) जो न तो पूरी तरह बेरोज़गार होती है, न ही स्थायी रूप से रोज़गार में। असल सवाल यह नहीं है कि देश में आबादी ज़्यादा है, बल्कि यह है कि सारी दौलत, ज़मीन, संसाधन कुछ अमीर लोगों के कब्ज़े में हैं। जो व्यवस्था हर साल अरबपतियों को पैदा करती है, लेकिन आधे देश को दो वक़्त की रोटी नहीं दे पाती वही व्यवस्था बेरोज़गारी की असली जननी है। इसलिए बेरोज़गारी का असली कारण ‘जनसंख्या’ नहीं, बल्कि वो आर्थिक व्यवस्था है जो मेहनतकशों को लूटकर अमीरों की दौलत बढ़ाती है।
बेरोज़गारी दर का असली मतलब क्या है?
बेरोज़गारी दर का मतलब समझते हैं: अगर सौ व्यक्ति काम करने के इच्छुक हैं काम करने के लायक़ भी हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन अगर उनमें से 6 व्यक्तियों को काम नहीं मिल पा रहा तो बेरोज़गारी की दर 6% हो जाएगी। ये दर किसी भी देश में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। developed कंट्रीज़ में ये 3% तक होती है, लेकिन सरकारी आँकड़ा यानी PLFS, Periodic Labour Force Survey, जून 2025 के मुताबिक़ भारत में कुल बेरोज़गारी दर 5.6% बतायी गई है। शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि सरकार ने बेरोज़गारी पता करने का फ़ॉर्म्युला ही बदल दिया है फिर भी ये दर 5% से नीचे नहीं आ सकी। इन्होंने क्या किया कि एक तो बेरोज़गारी दर Weekly Status के आधार पर निकाली है। यानी इस डेटा में पिछले 7 दिनों में जिसने 1 घंटा भी काम किया है उसे नौकरीवाला मान लिया है। या फिर उसने पिछले 1 साल में कम से कम 30 दिन कोई काम किया हो, तो भी उसे "नौकरीशुदा" मान लिया जाता है। बावजूद इसके 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोज़गारी दर 15.3% है। इतनी दर किसी देश में हो जाए तो सरकारें गिर जाती हैं। देश के बड़े-बड़े संस्थानों जैसे IITs तक में प्लेसमेंट गिर रहे हैं। बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में छंटनी की लहर चल रही है। TCS 12000 लोगों को बाहर करने वाली है। यानि अगर मिस्टर X ने पिछले हफ्ते सिर्फ एक घंटे के लिए कोई छोटा-मोटा काम किया, जैसे ठेला चलाया, खेत में पानी दिया, ट्यूशन पढ़ाया, या फिर पिछले साल में किसी महीने एक ठेके पर मज़दूरी की तो वो आदमी सरकारी आंकड़ों में बेरोज़गार नहीं माना जाएगा।
रोज़गार से जुड़ी एक अहम चीज़ होती है LFPR यानी Labour Force Participation Rate , यानी कितनी आबादी काम करने में या नौकरी ढूंढने में लगी है। सरकार की जून वाली रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का औसतन LFPR 54.2% है। यानि देश की आधे से ज्यादा आबादी किसी ना किसी तरह से रोज़गार से जुड़ी हुई मानी जाती है। OP Jindal के प्रोफेसर मोहन कहते हैं कि बेरोज़गारी दर कम होने का सीधा कारण है ‘Aspiration Gap’, आज के युवा ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, लेकिन बाज़ार में उतनी योग्य नौकरियाँ हैं ही नहीं। और यही वजह है कि युवा अब समझौता करने को तैयार नहीं हैं , वो छोटी या कमज़ोर नौकरियों को ठुकरा रहे हैं।
और सबसे डराने वाला सच तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन (ILO) ने पिछले साल ही सामने रखा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्रेजुएट्स के बीच बेरोज़गारी, अनपढ़ लोगों के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है।
PLFS रिपोर्ट: छह सालों में देश की बेरोज़गारी दर आधी से भी कम हो गई
सरकारी PLFS रिपोर्ट कहती है कि पिछले छह सालों में देश की बेरोज़गारी दर आधी से भी कम हो गई है। 2017-18 में ये 6% थी, और 2023-24 में गिरकर 3.2% पर आ गई।
लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई लोगों को अब पहले से ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही हैं?
या फिर हुआ ये है कि कागज़ों में बेरोज़गारी तो घटाई गई, लेकिन जो काम बढ़ा वो बिना सैलरी वाला काम है, जैसे खेत में मदद करना, घर में unpaid labor, या फिर वो छोटे-मोटे काम जो बस ज़िंदा रहने लायक पैसे देते हैं। तो नौकरी बढ़ी है या मजबूरी? क्योंकि जब नौजवान ग्रेजुएट होकर रिक्शा चला रहा हो, या कोई औरत घर-घर जा कर झाड़ू पोंछा कर रही हो तो उसे "कामकाजी" गिना जा रहा हो। इससे आँकड़े सुधर सकते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं। अगर असल में नौकरियाँ बढ़ रही होतीं, तो आज पढ़े-लिखे युवा सड़कों पर कांवड़ ना उठा रहे होते और लाखों डिग्रीधारी खाली बैठकर निराश न होते।
इसी दौरान सरकार ये भी बताती है कि LFPR 2017-18 में 49.8% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 60.1% हो गई है। फिर वही झूठ क्या ये बढ़ती संख्या वाकई अच्छी नौकरियों की है? खेतों में और घरों में बिना वेतन का काम भी 'रोज़गार' गिन लिया जा रहा है, जब रिक्शा चलाने, ऐप डिलीवरी करने या एक घंटे के ट्यूशन को भी जॉब मान लिया जाए, तो बढ़ती LFPR असल रोज़गार की नहीं, एक बढ़ते संघर्ष की कहानी बन जाती है। LFPR बढ़ने की एक वजह ये है कि अब ज़्यादा लोग ‘self-employed’ यानी खुद के दम पर किसी न किसी तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन 'self-employed' कहना भी अपने आप में एक भ्रम पैदा करता है। एक तरफ एक बड़ा उद्यमी है, जो करोड़ों का व्यापार चला रहा है वो भी self-employed कहलाता है। और दूसरी तरफ एक छोटा किसान है, जो किसी और की ज़मीन पर हल चला रहा है वो भी उसी कैटेगरी में आ जाता है।
लेकिन दोनों की ज़िंदगी देखिए आप, उनकी सिक्यरिटी जंचिए, और शोषण का स्तर देखिए, ज़मीन-आसमान का फर्क नज़र आएगा। जब रोज़गार का मतलब पेट पालना भर रह जाए तब आँकड़े ‘सकारात्मक’ लग सकते हैं, लेकिन हक़ीक़त अंदर से खोखली हो जाती है।
सरकारी आंकड़े फिर एक भ्रम पैदा करते हैं गाँवों में बेरोज़गारी दर शहरों से कम है। अगर हाँ, तो कैसे? शहर जहाँ इंडस्ट्री है, दफ्तर हैं, कंपनियाँ हैं वहाँ से ज़्यादा काम गाँवों में कैसे हो सकता है? सरकार इसका जवाब देती है खेती-किसानी अच्छा कर रही है, इसलिए गाँव में रोज़गार ज़्यादा है। अब आप सोचिए अगर कृषि क्षेत्र इतना अच्छा होता, तो न तो मजदूरी इतनी कम होती, न किसान कर्ज में डूबते। अब शहरों में महंगाई ज़्यादा है और जो युवा बड़े बड़े सपने लेकर शहर आए थे, वो जब देखते हैं कि न किराया दे पा रहे रहने का, ना सैलरी बढ़ रही तो घर वापस जाना पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि शहरों में LFPR और भी नीचे दिखता है क्योंकि जो लोग लौट गए, वो अब शहर के आंकड़े में नहीं हैं।
और मिडल क्लास सरकारों के मेनिफ़ेस्टो में नहीं हैं।